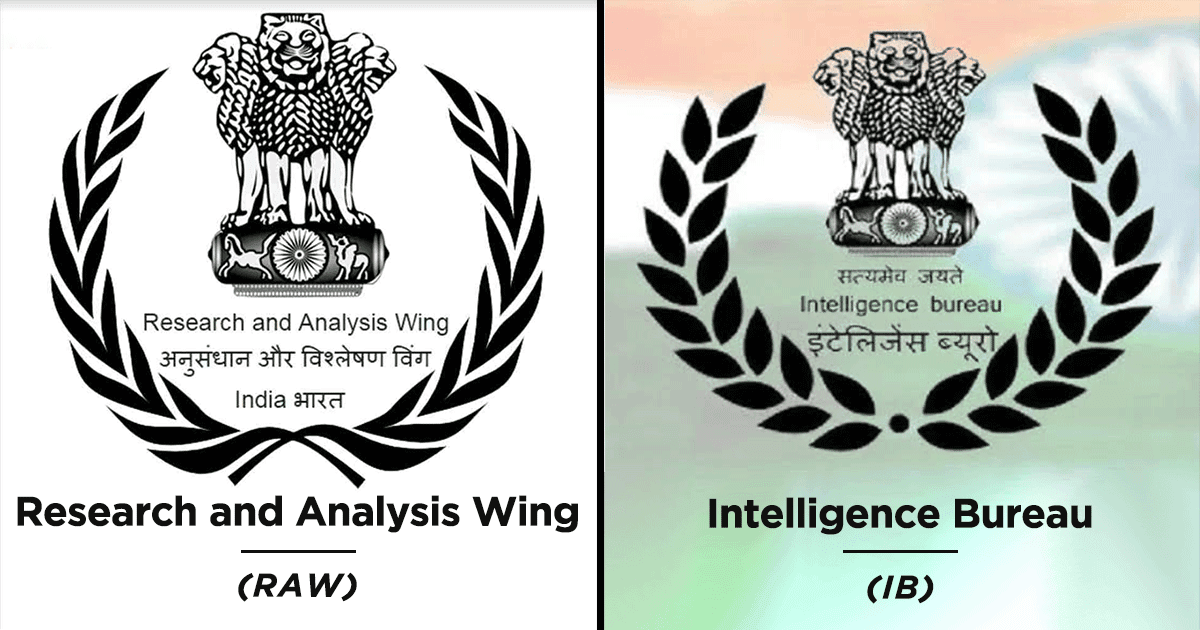उन दिनों मेरे गांव में बारी-बारी से बिजली आती थी. एक दिन… दिन में, एक दिन… रात में. पर कभी-कभी इन नियमों को ऊलट-पुलट भी कर दिया जाता था. गांव वालों को बिजली की दरकार इतनी नहीं रहती थी, क्योंकि नहर के पानी से भी फसलें अच्छी खासी पक जाया करती थी. बिजली के ज़्यादा मायने थे भी और नहीं भी. चांदनी रातों में लुका-छिप्पी का खेल बहुत खेला है मेरे बचपन ने. उन चांदनी रातों के बाद जब अंधेरी रातें आती थी, तो अंधेरा कीमती लगने लगता था. चूल्हा बुझने के बाद लोग अपना-अपना बिस्तर पकड़ लेते थे. धूनी सुलगती रहती थी, सारी रात धुआं उठता रहता था. मच्छरों से हम भी बचते थे और मवेशी (गाय,भैंस, बकरी आदि) भी.
उन्हीं दिनों कई तरह की अफवाहें फैलती थी, जैसे कि रात को चोर काला कच्छा पहन और तेल लगाकर चोरी करने आते हैं. दिन में फैली इन अफवाहों को सच मानकर रात को लोग पहरे देते थे. जागते रहो, जागते रहो के नारे लगते. स्कूल में पढ़ता था मैं, इतना याद है बस… क्लास कौन-सी थी ये नहीं पता. पता चला कि कल स्कूल में शहीदी दिवस मनाया जायेगा (23 मार्च को मनाया जाता है शहीदी दिवस). हमारे प्रिंसिपल साहब जट सिख थे. उन्होंने हमें थोड़ा-थोड़ा भगत सिंह के बारे में बताया. बताया तो उन्होंने शायद पूरा था, पर हमें थोड़ा-थोड़ा ही समझ आया. उस दिन मन में कई सवाल लिए मैं घर गया. जैसे कि शहीद कौन होते हैं? फांसी क्यों दी जाती है. भगत सिंह की मां कौन थी? ऐसे-वैसे कुछ-कुछ सवाल मेरे दिमाग के बस्ते में मेरे साथ ही घर को हो लिये.
मां ने मिलवाया जब भगत सिंह से
रात को मां खाना बना रही थी. चूल्हे पर थापियां (गोबर के उपले) सुलग रही थी. मां को खाना बनाने के साथ-साथ गाना गाने का बहुत शौक था और आज भी है. अगले दिन स्कूल में जो शहीदी दिवस पर प्रोग्राम था, उसके बारे में मैंने मां को बताया. मां ने पूछा कि, “तूने भाग लिया उस प्रोग्राम में”? मेरा जवाब था, “नहीं”.
मां ने मुझे भगत सिंह के बारे में बताना शुरु किया. किस्सा शुरु हुआ मनोज कुमार की फ़िल्म “शहीद” से. ये फ़िल्म मेरे नाना जी ने मेरी मां को दिखाई थी. इसका एक गाना मां ने मुझे सिखाया. खाना खाकर मां की छाती पर सर रख कर मैं वो गाना सीख रखा था. मेरा कान मां की छाती पर था. छाती से निकलती आवाज़ मेरे कानों के जरिए मेरे शरीर के रोम-रोम में बस रही थी. मैंने वो गाना सीख लिया.
गाने के बोल कुछ इस तरह थे:
इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर
इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर
आज इसी को पहन के निकला, पहन के निकला
आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला
माय रंग दे बसंती चोला.
मां ने ‘रंग दे बसंती चोला’ का मतलब भी समझाया. आज कई सालों के बाद भी ये गाना मुझे याद है. लेकिन भगत सिंह अभी बाकी था. मैंने अगले दिन स्कूल में वो गाना सबके सामने गाया. पता नहीं क्यों मेरी आखों में एक नमीं-सी आ गई. कुलजीत मैडम तो रोने ही लग गई थीं. उन्होंने गले लगाकर मेरी बलाईयां भी ली थी और मुझे गाना गाने पर संतरे वाली टॉफियां भी दी थी. घर आकर मां को मैंने बताया तो वो बहुत खुश हुई. उस रात मां ने मुझे एक और गाना सिखाया.
ऐ वतन, ऐ वतन हमको तेरी क़सम
तेरी राहों में जां तक लुटा जायेंगे
फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम
भेंट अपने सरों की चढ़ा जायेंगे
ऐ वतन, ऐ वतन
मैं अभी भगत सिंह के नाम से मिला था, काम से मिलना अभी बाकी था. मां ने बताया कि भगत सिंह एक ऐसा क्रांतिकारी था, जिसने हम सबके लिए सिर्फ़ 23 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया. हालांकि मां ने इस अंदाज़ में नहीं बताया था. इन सबके कुछ दिनों के बाद ही एक दिन स्कूल से घर वापिस आया तो “शहीद” फ़िल्म आ रही थी. प्रेम चोपड़ा, मनोज कुमार और अन्नत पुर्षोतम मराठे मुख्य भूमिका में थे. पूरी फ़िल्म के दौरान मेरे अंदर कुछ उबलता रहा. अतं में एक सीन आता है.
जहां जेलर पूछता है: भगत सिंह तुम्हारी कोई आख़िरी ख्वाहिश”?
मनोज कुमार (जो भगत सिंह का किरदार निभा रहे थे): “हमारे हाथ खोल दिए जायें. हम एक-दूसरे के गले मिलना चाहते हैं. अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलेंगे.”
जेलर: “खोल दो”
हाथ खोलते ही तीनों गले मिलते हैं. पीछे से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब ज़िंदाबाद के नारे लगते हैं. इस सीन ने मुझे बहुत परेशान किया. मैं रोने लगा. बहुत रोया अपनी मां के गले लग कर. ऐसे लगा जैसे भगत सिंह और उसके साथी मेरे अपने हों, इतने अपने कि उतने अपने भी नहीं. मां ने बहादुरी के बहुत से किस्से सुनाये, पर इन किस्सों ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया, परेशान कर दिया. कई दिनों तक ये परेशानी चलती रही. कुछ-कुछ होता रहा. सपने बहुत आते थे उन दिनों. जिस चीज़ के बारे में सोचो वो सपनों में मिलने लगती थी. पर भगत सिंह मेरे सपने में कभी नहीं आया. ना जाने क्यों कभी-कभी सोचता हूं कि वो सपनों में नहीं, हकीकत में मेरे ही नहीं, बल्कि सब के साथ कहीं ना कहीं खड़ा रहता है.