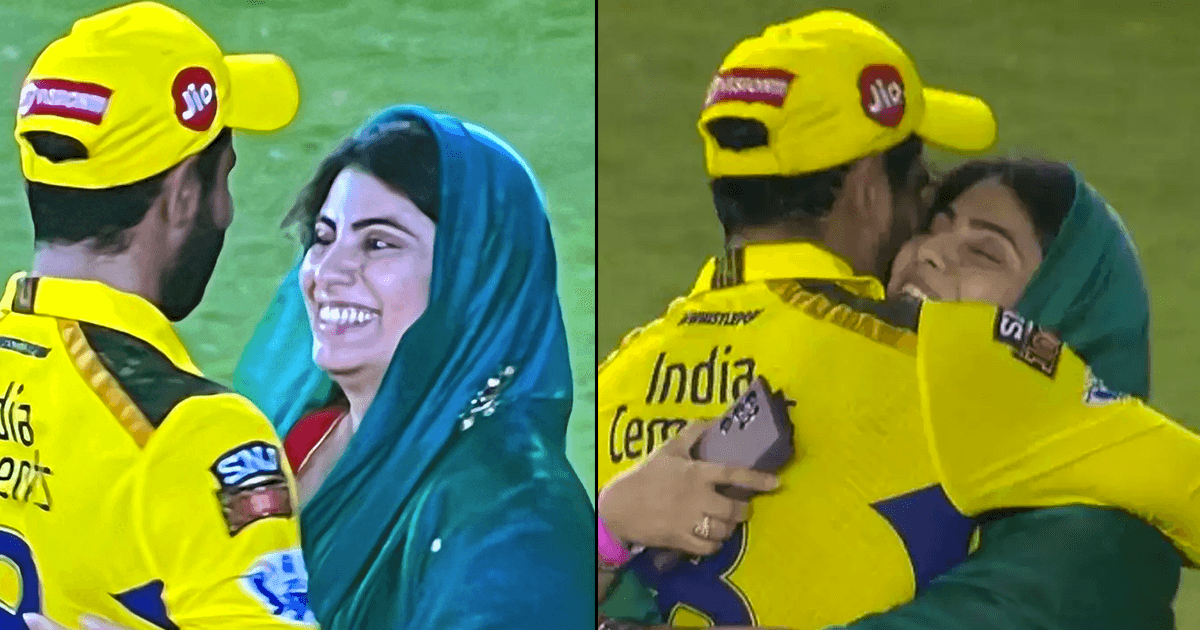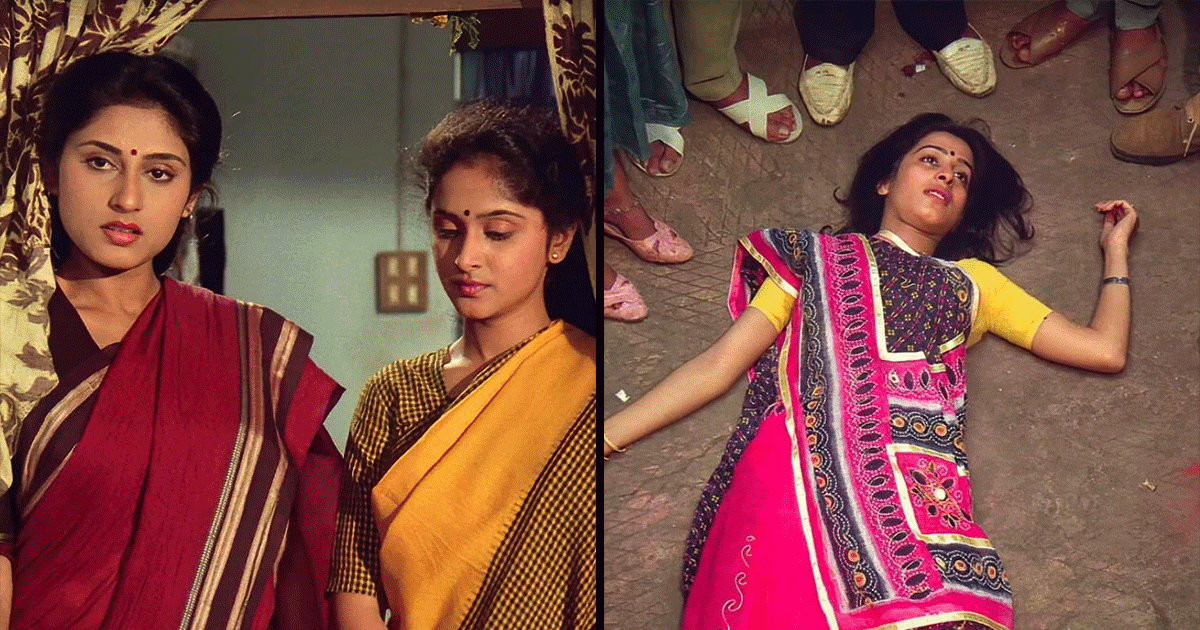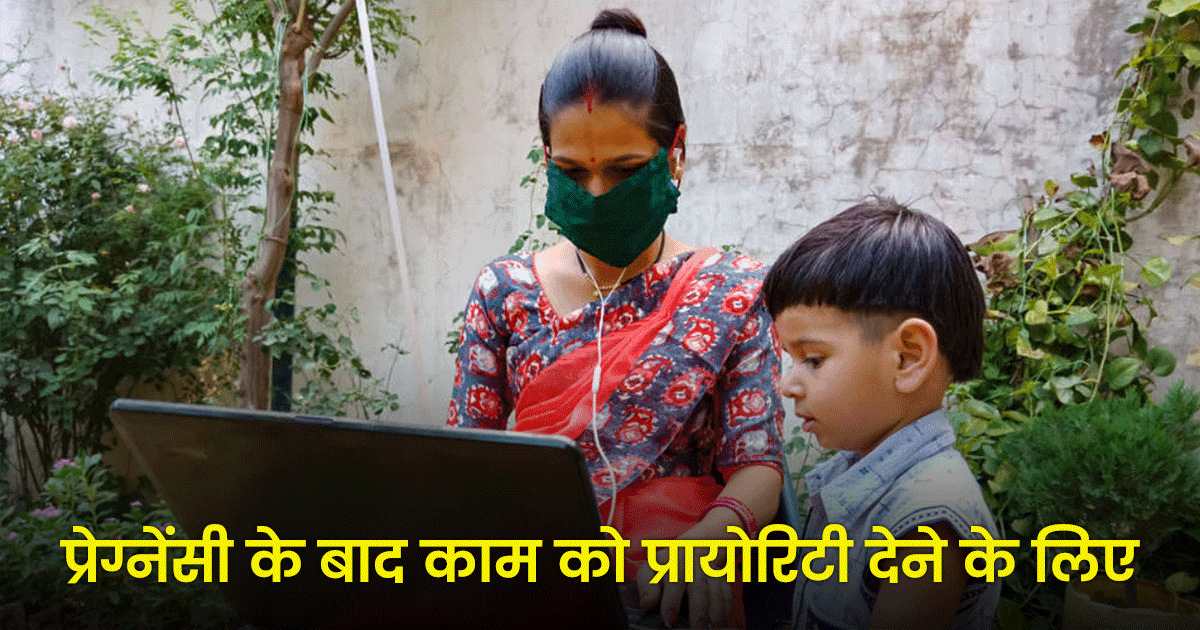शनिवार की ये सुबह हर आम सुबह की तरह ही आम थी. बस हल्की हवाओं के साथ होती धीमी-धीमी बारिश किसी बॉलीवुडिया फ़िल्म की तरह मौसम को बेईमान करने लगी थी. मौसम की इस बेईमानी को देख कर दिल करने लगा कि छोड़ो यार घर निकलते हैं, नेट पर ही रेख़्ता देख लेंगे. फिर ख़्याल आया कि नेट पर तो रेख़्ता को देखा जा सकता है. पर गुलज़ार और जावेद साहब जैसी हस्तियों से न जाने फिर कब रूबरू होने का मौका मिले.
ऐसे ही कई ख़्यालों में डूबा आख़िरकार मेट्रो के लिए निकल ही पड़ा. ये ख़्याल भी कितने हसीं होते हैं, जो कभी किसी के इतने करीब ले जाते हैं, जिसे हक़ीक़त में भी कभी आपका ख़्याल नहीं आया होता. तो कभी उन निगाहों की ढेर सारी बातें करवा देते हैं, जो एक-दूसरे को देखते ही खामोश होकर झुक जाया करती हैं. खैर ख़्यालों पर कब किसका ज़ोर चला है, जो अपना चलने वाला है? ऐसे ही ख़्यालों में डूबा मैं भी जश्न-ऐ-रेख़्ता के सालाना जलसे में नई दिल्ली के ‘Indira Gandhi Centre for the Arts’ पहुंचा. यहां पहुंचने से पहले उम्मीद थी कि उर्दू के चाहने वालों एक हुजूम मुझे यहां नज़र आने वाला है. पर यहां सिर्फ उर्दू से प्रेम करने वाले ही नहीं बल्कि उर्दू न जानने वाले लोगों की भी भरमार थी.
मंच पर सफ़ेद कुर्ते पर हलके क्रीम कलर की शॉल ओढ़े गुलज़ार साहब को देखने और सुनने के लिए क्या बच्चे और क्या बुज़ुर्ग ऐसे एक-दूसरे पर चढ़े हुए थे, मानों सब किसी खुले खज़ाने को लूटने की ताक में बैठे हों. पर ये भी एक हक़ीक़त ही है कि गुलज़ार साहब किसी खज़ाने से कम नहीं. खैर, जब गुलज़ार साहब को अपने इतने करीब देखा तो दिल करने लगा कि भाग कर उस शख़्स के करीब जाऊं और उसके कदम चूम लूं, जिसने ‘मोमिन’ से ले कर ‘मीर-तक़ी-मीर’ और ‘मिर्ज़ा ग़ालिब’ के कलामों को लोगों की ज़बान तक पहुंचाया और गुम होती उर्दू ज़बान के दौर में भी उन्हें ज़िंदा रखा. खैर सोचने का क्या है? इसके कौन से पैसे लगते हैं, यही तो एक चीज़ है, जो इस महंगाई के दौर में भी फ्री मिल जाती है. गुलज़ार साहब भी अपनी कविताओं के ज़रिये दर्शकों और चाहने वालों का इस्तकबाल करते रहे.
आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जिसका मैं और मेरे जैसे बहुत से चाहने वालों को बेसब्री से इंतज़ार था, गुलज़ार साहब ने जैसे ही अपनी कविता ‘लम्हें और ऐश ट्रे’ को सुनाने के लिए कागज़ को उठाया, वैसे ही दर्शकों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, लोगों की चिल्लाहट ने माइक की आवाज़ को जैसे कहीं दबा दिया. पर गुलज़ार साहब की बुलंद आवाज़ के साथ ही वो अचानक पनपा शोर कहीं दूर उठे धुंए-सा गायब हो गया.
‘मेरे ऐश ट्रे में हैं कुछ बुझे हुए लफ़ज़ और लफजों में समाये हुए चंद…’
इन अल्फ़ाज़ों के साथ गुलज़ार साहब से विदा लेते हुए मैं Amphitheatre पहुंचा, जहां जावेद अख़्तर एक बुक लांच के मौके पर शबाना आज़मी के साथ आये हुए थे. आर्ट सिनेमा से लेकर कमर्शियल फ़िल्मों में अपने जौहर दिखा चुके इस दंपत्ति को एक साथ एक मंच पर देखना अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव था.
यहां आने के बाद ही यह पता चल पाया कि ‘अंकुर’, ‘निशांत’ जैसी गंभीर फ़िल्मों में गंभीर व्यक्ति का किरदार निभाने वाली शबाना असल ज़िंदगी में एक जिंदादिल शख़्सियत हैं. दर्शकों के बीच वो घास पर कुछ इस कदर बैठ गईं, मानों वो कोई बड़ी हस्ती नहीं बल्कि भीड़ का ही एक हिस्सा हो.
जावेद साहब की नज़्म और शबाना आज़मी की साथ में गूंजती तालियां, दिल ये दुआ कर रहा था कि काश ये वक़्त बस यहीं ठहर जाए. पर वक़्त भला कभी किसी के लिए कहां रुका है, जो कमबख्त मेरे लिए रुकेगा? इस तरह शनिवार की एक आम शाम मेरे लिए कुछ ख़ास एहसासों को छोड़ते हुए बीत गई.
शनिवार रात की खुमारी अभी उतरी नहीं थी इसलिए रविवार की सुबह भी आंख ज़रा देर से खुली. मोबाइल पर नज़र पड़ी तो याद आया कि आज वैलेंटाइन डे है. पर अब कोई ऐसा था भी नहीं, जो कॉल करके ये याद दिलाता कि आज वैलेंटाइन है और मिलना भी है. खैर सिंगलपने के मारे हम एक दोस्त को लेकर जश्न-ऐ-रेख़्ता की ओर ही निकल लिए. वहां पहुंचने से पहले उम्मीद थी कि आज वैलेंटाइन डे की वजह से कई लोग तो जो कहीं और जश्न मना रहे होंगे और हमे भीड़ कम मिलेगी. पर यहां पहुंचें तो नज़ारा ही दूसरा देखने को मिला. बुजुर्गों से ज़्यादा तो हमें यहां युवा नज़र आये, जो अपना वैलेंटाइन उर्दू और जश्न-ऐ रेख़्ता के साथ मानाने आये थे.
प्रोग्राम के शेडयूल को देख कर मालूम हुआ कि आज मुन्नवर राणा और कुमार विश्वास एक ही स्टेज पर लोगों के साथ गुफ़्तगू करने वाले हैं. अफरा-तफरी में हम भी लॉन तक पहुंचें पर कुमार विश्वास को अकेले पाकर थोड़ी निराशा हुई. जब कुमार विश्वास अपने चिर परिचित अंदाज़ में आये तो वो निराशा भी कहीं दूर हो गई. पगली लड़की एक बार फिर कुमार के ज़रिये ज़िंदा हो चुकी थी. लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कुमार ने फैज़ से लेकर फ़िराक़ और अकबराबादी के क़लामों को पढ़ा और आज के दौर में उनकी रचनाओं की उपयोगिताएं बताई.
इसके बाद वो पल भी आ गया, जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था. ‘फ़िल्मों में उर्दू’ पर बात करने के लिए जावेद अख़्तर समेत जावेद सिद्द्की, इम्तियाज़ अली और तिग्मांशु धूलिया स्टेज पर इकट्ठे हुए थे. जहां उन्होंने आज की फ़िल्मों में उर्दू के महत्व पर बात करते हुए कई ऐसी बातें साझा की जो किसी आम जीवन में बिलकुल सामान्य सी बात हैं पर फ़िल्मों में उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है.
इसके बाद लोगों के सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ. जहां कुछ मतभेद भी सामने निकल कर आये. पर ये मतभेद भी तो ज़रूरी ही हैं, इससे देखने वालों को याद रखने का एक बहाना मिल जाता है. प्रोग्राम के बाद बाहर निकले तो टॉम अलटर से मुलाकात हुई. उम्र के जिस पड़ाव पर आने के बाद लोग परमात्मा को याद करने में जुट जाते हैं, उस उम्र में भी टॉम लोगों के साथ फुटबॉल की बातें करते हुए दिखें.
कुछ ऐसी ही चीज़ों को अपनी यादों के पिटारे में कैद किये हुए जब मैं गेट से बाहर आया तो सोचने लगा कि एक प्राइवेट संस्था होने के बावजूद जब रेख़्ता, जश्न-ऐ-रेख़्ता जैसे कार्यक्रम के ज़रिये उर्दू के चाहने वालों के साथ उर्दू अदब को मरने से बचा सकता है, तो सरकार के तमाम संसाधनों के बावजूद भारतीय भाषाएं हाशिये पर क्यों पड़ी है?