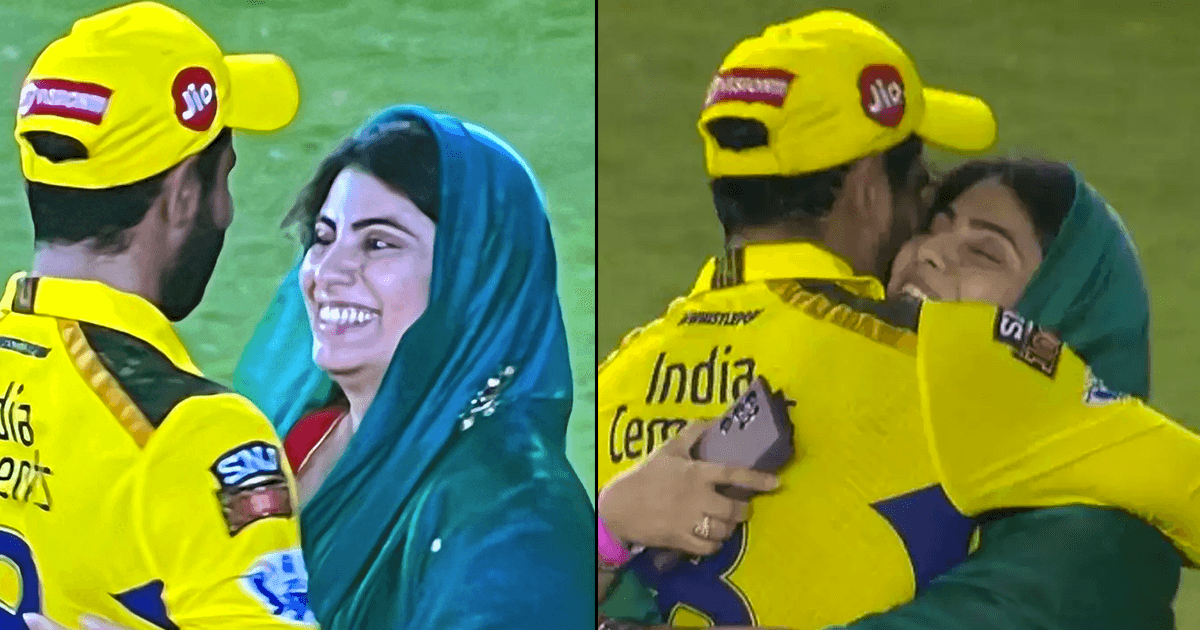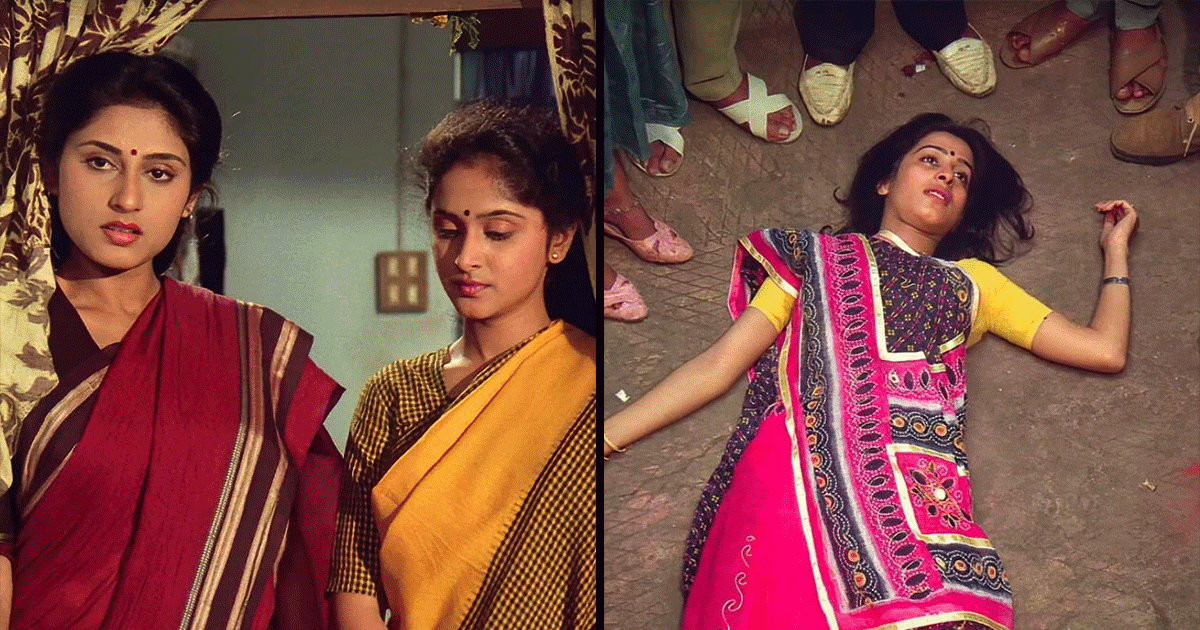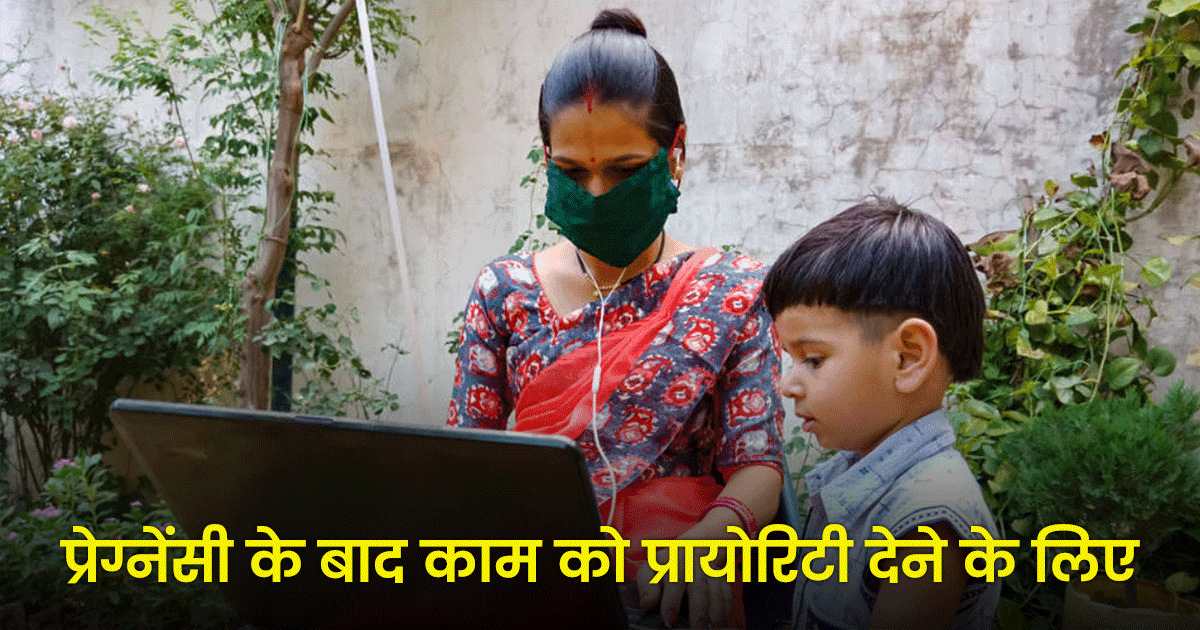पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. लोकतंत्र के महापर्व में पांच राज्यों के नेता डुबकी लगाने को तैयार बैठे हैं. लेकिन डुबकी लगाने से पहले वो बहुत सारे राजनीतिक पाप करना पसंद करेंगे. चुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक पार्टियों के बीच तू डाल-डाल, मैं पात-पात का खेल शुरू हो गया है. पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नतीजों पर टिकी हैं. ऐसा लोग कहते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुज़रता है. अगर ऐसा है, तो फिर राजनीतिक सड़क (रास्ता) निर्माण में अथाह पैसे की आवश्यकता होगी और पार्टियां दिल खोलकर पैसे लुटाएंगी. अब चुनाव के नतीजों तक नेताओं के पैर ज़मीन पर नहीं टिकेंगे. अब वो रोज़ उड़नखटोलों की सवारी कर छोट- भइया नेताओं द्वारा इकट्ठा की गई भीड़ को संबोधित करने आएंगे. मेनिफेस्टों के नाम पर लॉलीपॉप थमाएंगे और एक बार फिर से आम जनता (वोटर्स) को उनकी औकात बताएंगे.

पैसों से होता है हार-जीत का निर्धारण
पहले के चुनावों में उम्मीदवारों की हार-जीत का फ़ैसला जनता-जनार्दन के हाथों में हुआ करता था. मगर अब राजनीतिक दृश्य ही नहीं बदले हैं, बल्कि पूरा समीकरण बदल गया है. अब हार-जीत का फ़ैसला खुद राजनीतिक पार्टियां और नेता करते हैं. मतलब चुनावों में जो जितना पैसा खर्च करता है, जीत उसी की होती है. यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही है कि अब भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सत्ता का निर्धारण पैसों से होता है. शायद यही वजह है कि चुनाव आते ही पार्टियां और नेता दिल खोलकर पैसे लुटाते हैं. चुनाव जीतने के लिए धनबल का इस्तेमाल करते हैं और पैसों से जनता क्या, अब तो प्रशासन को भी मैनेज कर लेते हैं. जनता को लोक-लुभावन बातों से फुसला लेते हैं और सत्ता की गद्दी पर काबिज़ हो जाते हैं. अब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा सब में यही खेल होता है और ऐसे ही कुछ फॉर्मूले अपनाये जाते हैं, जिनसे सत्ता की कुर्सी पाई जा सके.
भारत में बदल गया है चुनाव का स्वरूप
दरअसल, भारत में चुनाव का मतलब हो गया है पैसों की गंगा बहाना. शुरू से ही चुनाव, नेता, रैली और जनता भारतीय लोकतंत्र के धुरी रहे हैं. धुरी तो अभी भी हैं, मगर अब उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है. अब चुनावों में वो पहले वाली बात नहीं रही, जिसमें जनता स्वत: स्फूर्त होकर इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जाती थी. पहले समाज के लोग नेताओं के चयन को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर घूम कर सही उम्मीदवार के पक्ष में बिना किसी स्वार्थ के लोकमत का निर्माण करते थे. मगर अब राजनीति का पहिया पलट चुका है. चुनाव का मतलब भी बदल गया है. नेता बदल गये हैं. मुद्दे बदल गये हैं. विचार बदल गया है. सामाजिक ताना-बाना बदल गया है. और यहां तक कि चुनावी रैलियों का स्वरूप भी बदल गया है.
रैलियों में पैसों से भीड़ को इकट्ठा किया जाता है
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र लखनऊ में महारैली की थी, जिसमें बीजेपी ने ऐसा दावा किया था कि इस रैली में लगभग 5 लाख लोगों ने भाग लिया. पीएम मोदी की रैली को सफ़ल बनाने में बीजेपी ने जमकर पैसे खर्च किये. अगर सूत्रों की मानें, तो इस रैली में लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए करीब 16 करोड़ रुपये खर्च किये गये… जी हां, 16 करोड़ रुपये. महज एक रैली को आयोजित करने में जब पार्टी को करीब 16 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े, तो अब इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पांचों राज्यों के चुनावों के मद्देनज़र सभी पार्टियां जब अंधाधूंध रैलियां करेंगीं, तो किस तरह से पैसों की नदियां बहाई जाएंगी. और यह रकम इतनी अधिक होगी, जिसकी एक भी पाई देश और समाज के विकास पर खर्च नहीं होगी. अब रैली में जनता को बसों में ठूंस-ठूंस कर लाया जाता है. इतना ही नहीं, उन्हें एक दिन के पैसे भी दिये जाते हैं और खाने-पीने की तो बात ही मत कीजिए. नेता, विधायक और सांसद अपने-अपने आवास पर जनता को मेहमान की तरह रखते हैं. रैली का स्वरूप बताने के लिए बस इतना ही काफ़ी है.

जनसभा या चुनावी रैली अब चुनावी इवेंट बन गया है
मगर बात सिर्फ़ बीजेपी की नहीं है. देश की दूसरी पार्टियां मसलन, कांग्रेस, बसपा, सपा, जदयू और राजद सरीखीं और भी पार्टियां हैं, जो चुनावों को जीतने और रैलियों को सफ़ल बनाने के लिए पैंसों का मोह छोड़ देती हैं और पैसे बांट कर रैलियों में लोगों की भीड़ इकट्ठा करती हैं. चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां ‘एक ही थाली के चट्टे-बट्टे’ बन जाते हैं. इसलिए अब चुनावों में रैली अथवा जनसभाएं नहीं होतीं, बल्कि इवेंट होता है, जिसके लिए हर राजनीतिक पार्टी की एक अलग टीम होती है, जो इस रैलीनुमा इवेंट को बड़े लेवल पर ऑर्गनाइज़ करती है. अगर आप पैसों से जुटाई गई भीड़ को रैली का नाम दे रहे हैं, तो आप ग़लत हैं. क्योंकि पैसों से रैलियां आयोजित नहीं होतीं, बल्कि इवेंट्स आयोजित होते हैं. इवेंट, जिसमें आने वाले लोगों को न्योता दिया जाता है, उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम होता है, उनके रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था होती है और जाने के वक़्त कुछ पैसे भी दिये जाते हैं, ताकि वो लोग इवेंट के ऑर्गनाइज़र (नेता) की चर्चा करते न थकें.
रैली में लोग स्वत: नहीं आते, बल्कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी टीम होती है
जनसभा अथवा रैलियों की अवधारणा तो आज से कई दशक पहले हुआ करती थीं. जिसमें नेताओं के एक आह्वान पर लोगों का हुजूम टूट पड़ता था. जब रैलियों का नाम लोग सुना करते थे, तो नेताओं को देखने, उनके विचार और भाषण को सुनने स्वत: स्फूर्त जाया करते थे. जिसे जो सवारी मिलती थी, मसलन, बस, ट्रक और रेल किसी पर भी लटक जाया करते थे, खाने की एक पोटली अपने साथ रख लिया करते थे और चल देते थे अपने आदर्श नेता और पार्टी की रैलियों में. मगर आज वो स्वत: स्फूर्त वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलतीं. याद रहे वो रैली हुआ करती थी, कोई इवेंट नहीं. आज की तरह रैलियों को सफ़ल बनाने के लिए राजनीतिक पंडितों, आईटी के जानकारों और जनसंपर्क के लोगों की टीम को कई स्तर पर कार्यालय बनाकर नहीं रखा जाता था. रैलियों के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापनों पर इतना खर्च नहीं किया जाता था. सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं चलाया जाता था. पहले लोग नेताओं के चेहरे पर खुद रैली में जाया करते थे. आज की तरह इवेंट मैनेजर नहीं होते थे और न ही कोई जनसंपर्क पदाधिकारी होता था, जो इवेंट को सफ़ल बनाने की ज़िम्मेदारी लेता था.

पहले चुनावी इवेंट नहीं, रैली- जनसभा हुआ करती थीं
अगर भारत के राजनीतिक इतिहास पर ज़रा नज़र डालेंगे, तो आपको ऐसे कई मौके मिलेगें, जहां पर आपको रैली का महत्व और उनका सकारात्मक स्वरूप नज़र आयेगा. साल 1939 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी नई पार्टी ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ की पहली रैली पटना के गांधी मैदान में की थी, तो इस रैली में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था. भारत की आज़ादी के पहले जब महात्मा गांधी एक आवाज़ देते थे, तो पूरा देश उनके साथ खड़े होकर चलने को तैयार हो जाता था. महात्मा गांधी ने पटना के गांधी मैदान में व्यक्तिगत तौर पर कई ऐतिहासिक रैलियां कीं, जिनमें जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया. अगर अभी भी आपको रैलियों के असल स्वरूप का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, तो ज़रा एक बार जयप्रकाश नारायण को याद कर लीजिए. 5 जून, 1974 को गांधी मैदान में ही जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद किया था, तो घरों में बैठे लोग सारा काम-धंधा छोड़ कर गांधी मैदान में भर आए थे. उनके एक आह्वान पर सारा देश उठ खड़ा हुआ था. याद रहे, ये कोई इवेंट नहीं था और न ही पैसों से जुटाई गई भीड़.
मगर अफ़सोस अब हमारे देश में न तो ऐसे कोई नेता रहे और न ही कोई ऐसी राजनीतिक पार्टियां, जो अपने चेहरे और विचार के दम पर लोगों को बिना किसी ताम-झाम के एक जगह इकट्ठा कर लें. जब नेताओं ने ईमानदारी की चादर ओढ़ना छोड़ दिया, तो लोगों ने भी अपनी ईमानदारी के चोले को उतार फेंका.

चुनावों में खर्च होने वाले आंकड़ें चौंकाने वाले हैं
सच कहूं, तो अब पैसा है, तो चुनाव है. अगर पैसा नहीं तो चुनाव नहीं. अगर आंकड़ों की बात करें, तो ऐसा अनुमान है कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 30 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए. मतलब भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक का सबसे खर्चीला चुनाव. चुनावी खर्चे पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडी (सीएमसी) के अनुसार, 1996 में लोकसभा चुनावों में 2500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. साल 2009 में यह रकम बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गई. इसमें वोटरों को गैरक़ानूनी तरीके से दिया गया कैश भी शामिल है.
तय सीमा से अधिक खर्च करते हैं उम्मीदवार
सबसे खास बात ये है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा तय करने का बाद भी नेता और पार्टियां मानने को तैयार नहीं हैं. चुनाव आयोग राज्यों के अनुसार चुनावों में खर्च होने वाले धन की सीमा तय कर देती है. इस बार भी यूपी चुनाव में यह सीमा प्रति उम्मीदवार 28 लाख रुपये तय कर दी गई है, मगर जिस तरह से रैलियों का शंखनाद हो रहा है और वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में नेताओं के बीच होड़ लगी है, उससे कहीं नहीं लगता कि चुनाव आयोग के फ़ैसले का सम्मान होगा, उल्टे उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी.
राजनीतिक पार्टियां के साथ-साथ हम भी हैं जिम्मेदार
वैसे इन सबके लिए न तो सिर्फ़ नेता जिम्मेदार हैं और न ही राजनीतिक पार्टियां. जिम्मेदार कोई है, तो वो हैं हम आमलोग, जो ज़रा सा प्रलोभन में पड़कर ये भूल जाते हैं कि हमारे संविधान ने हमें लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मतदान के अधिकार के रूप में कितना बड़ा हथियार दिया है. सच कहूं, तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोकतंत्र पर लगे दाग को साफ़ करने की जिम्मेवारी अब हम नागरिकों पर आ गई है. अगर हम खुद संभल जाएं, तो हमारे और आपके पैसों को जिस तरह से चुनाव और उसकी तैयारियों के नाम पर बहाया जाता है, वो हमारे विकास के काम में आ सकेगा. अगर रैलियों को इवेंट बनने से रोक देंगे, तो उसमें खर्च होने वाले पैसे देश के विकास में सहायक होंगे. बाकी तो सब आप जनता-जनार्दन पर निर्भर करता है.